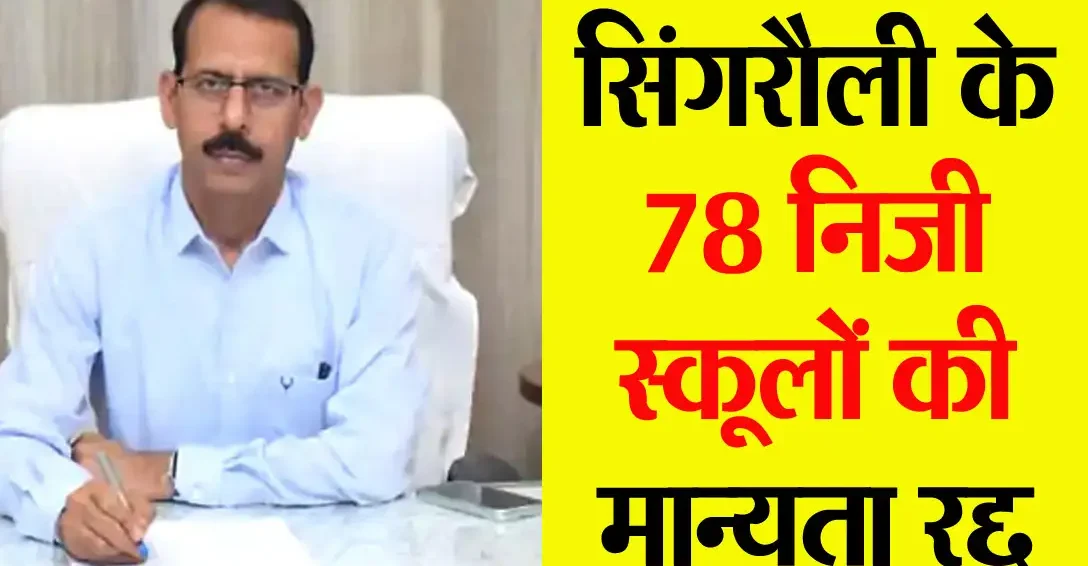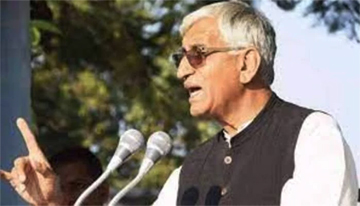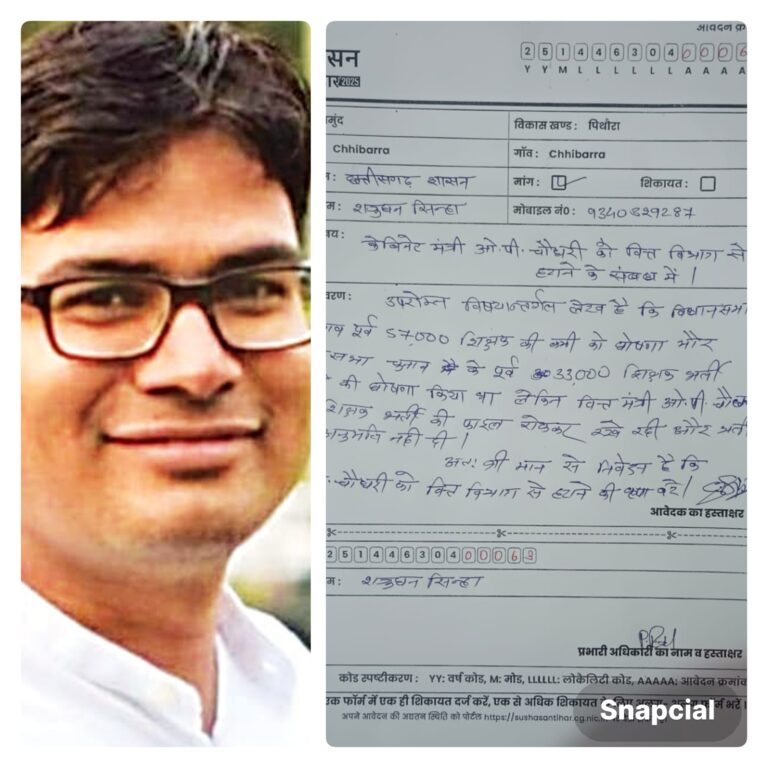भारत एक अमीर गरीब देश है. मतलब कि देश के ज्यादातर लोग अमीर हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या गरीबों की भी है.
भारत में पिछले 75 सालों से अलग अलग राजनीतिक पार्टियां गरीबी से जुड़े नारे देकर सत्ता में आती रही हैं. 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर सरकार बनायी थी. उनके बाद राजीव गांधी ने भी यही नारा दिया और देश के प्रधानमंत्री बने. फिर 2014 में नरेंद्र मोदी ने भी देश से गरीबी हटाने के कई वादे किए थे.
अब एक बार फिर देश में अगले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. चुनाव से पहले संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का एक ही लक्ष्य है- देश में कोई भी गरीब भूखा न सोए. इस स्लोगन के जरिए मोदी सरकार भारत के 80 करोड़ लोगों को एक साथ साधना चाहती है.
भारत को आजाद हुए 75 साल से भी ज्यादा हो गए. इस दौरान देश ने 12 प्रधानमंत्री देखे. लेकिन गरीबी और भुखमरी का मुद्दा ज्यों का त्यों रहा. हाल ही में नीति आयोग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले कुछ सालों में गरीबी का स्तर तेजी से कम हुआ है.
नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रमण्यम का कहना है कि पिछले कुछ सालों में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोग काफी ज्यादा समृद्ध हुए हैं. इतना ही नहीं दोनों क्षेत्रों के बीच के खर्च में भी ज्यादा फर्क नहीं रह गया है.
नीति आयोग की इसी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2013-14 में भारत की 29.17 प्रतिशत आबादी एमपीआई (बहुआयामी गरीबी सूचकांक) के हिसाब से गरीब थी. जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में घटकर 11.28 प्रतिशत हो गया है. यानी एमपीआई के अनुसार इन नौ सालों में 17.89 प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर आए है.
इन आंकड़ों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि इन तीन दशकों में गरीबी हटाओ के नारे को जीवंत बनाने के लिए जबर्दस्त तेजी दिखाई गई है. लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है.
कुछ अर्थशास्त्रियों का दावा है कि इस रिपोर्ट में पूरी तस्वीर पेश नहीं की गई है. 2022 में आई ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) की लिस्ट के अनुसार भी भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर है.
ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर भारत में वाकई गरीबी खत्म हो रही है तो हंगर इंडेक्स में देश की दशा इतनी बुरी क्यों है?
पहले समझिए कौन लोग हैं जो गरीब है
यूं तो ‘गरीब’ शब्द को परिभाषित करने के लिए कई पहलू जिम्मेदार होते हैं. लेकिन आमतौर पर जो अपनी बुनियादी जरूरत पूरी न कर सके, उन्हें गरीब की श्रेणी में रखा जाता है.
भारतीय योजना आयोग के अनुसार, कैलोरी की मात्रा को गरीबी के मापदंडों के रूप में माना गया है. ग्रामीण इलाकों में 2400 कैलोरी और शहरी इलाकों में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले लोगों को गरीब माना जाता है.
भारत में गरीबी मापने के दूसरे भी पैमाने हैं. नीति आयोग की तरफ से जो लिस्ट जारी की जाती है, उसमें MPI के आधार पर लोगों को कैटेगरी में बांटा जाता है. MPI गरीबी को स्वास्थ्य, शिक्षा और लाइफ़ स्टाइल के कुछ महत्वपूर्ण और बुनियादी मानकों के आधार पर परिभाषित करती है.

ये एमपीआई यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक है क्या ?
9 साल पहले यानी 25 सितंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 एसडीजी (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) तय किया गया था. एसडीजी का सबसे बड़ा मकसद गरीबी को जड़ से उखाड़ फेंकना था. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ये भी साफ़ कहा गया था कि गरीबी किसी एक मानक से तय नहीं की जा सकती. यही कारण है कि MPI को विकसित किया गया.
एमपीआई से यूएन को दुनियाभर के देशों में गरीबी की स्थिति का आकलन करने में मदद मिलती है. कुछ अलग-अलग इंडिकेटर के आधार पर MPI की गणना की जाती है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसका एक लेखा-जोखा भी बनाया है. हालांकि अपनी स्थिति के अनुसार हर देश इन इंडिकेटर में थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं.
अब समझिए की भारत में एमपीआई की गणना कैसे की जाती है
भारत में एमपीआई की गणना 12 इंडिकेटर के आधार पर की जाती है. इन 12 मापदंडों में पोषण, स्कूली शिक्षा के साल, प्रेग्नेंसी के दौरान देखभाल, बाल और किशोर मृत्यु दर, खाना पकाने में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है और स्कूल में उपस्थिति जैसे इंडिकेटर्स शामिल हैं.
इन 12 मानदंडों में स्वच्छता, किन घरों में बिजली है. किन घरों में पीने के पानी की उपलब्धता है, घर है या नहीं, संपत्ति कितनी है और बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाता है या नहीं, भी शामिल किया गया है.
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने गरीबी का 4 पैमाना बताया है, जिसे पूरा नहीं कर पाने वाले लोगों को गरीब माना गया है.
1. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता
2. टेक्नोलॉजी तक पहुंच
3. काम के अवसर, सैलरी और काम का ढंग
4. सामाजिक सुरक्षा